हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर
हैदर अली और टीपू सुल्तान का योगदान भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अठारहवीं शताब्दी के भारत में, उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों में सैन्य साहसी उभर रहे थे। इस समय, हैदर अली (जन्म 1721) जैसे लोग सामने आए। उसने एक साधारण घुड़सवार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे मैसूर का शासक बन गए। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर ने न केवल युद्ध में सफलता प्राप्त की, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी अपने दुश्मनों को हराया।
मैसूर का संघर्ष और हैदर अली का उदय
वाडियार राजवंश के शासक चिक कृष्णराज के गद्दी पर क़ब्ज़ा करने की प्रक्रिया 1731 से 1764 तक चली। इस दौरान, दो भाई, देवराज (मुख्य सेनापति) और नांजराज (राजस्व और वित्त के नियंत्रक) राज्य में वास्तविक शक्ति रखते थे। दक्षिण भारत में मराठों, निज़ाम, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच चल रहे संघर्षों ने मैसूर को भी इस राजनीतिक खेल में शामिल कर लिया।
साल 1753, 1754, 1757 और 1759 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, जबकि साल 1755 में निज़ाम ने भी हमला किया। इन हमलों और वित्तीय दावों के कारण, मैसूर आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। इस स्थिति ने राजनीतिक रूप से मैसूर को साहसी सैन्य कार्यों के लिए एक उपजाऊ भूमि बना दिया। देवराज और नांजराज को इस कठिन परिस्थिति का सामना करने में कठिनाई हो रही थी। इस समय, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो सैन्य कौशल, कूटनीतिक क्षमता और नेतृत्व में माहिर हो। 1761 तक हैदर अली ने मैसूर का वास्तविक शासक बनकर सत्ता अपने हाथ में ले ली।
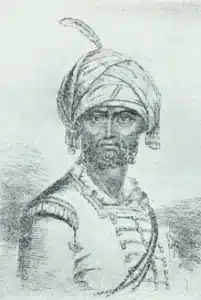
हैदर अली की रणनीति और सैन्य तैयारी
हैदर अली ने समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार किया। वह जानता था कि मराठों की सेना को हराने के लिए एक मजबूत और तेज घुड़सवार सेना की आवश्यकता है। साथ ही निज़ाम की फ्रांसीसी-प्रशिक्षित सेनाओं को मात देने के लिए एक प्रभावी तोपख़ाने की आवश्यकता थी।
वह पश्चिमी देशों के शस्त्र निर्माण के उन्नत ज्ञान से भी परिचित था। फ्रांसीसी सहायता से, हैदर अली ने दिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया। इस शस्त्रागार ने उसे अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति की। इसके साथ ही, वह पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण विधियों से भी लाभान्वित हुआ। इन सभी प्रयासों से, हैदर अली ने सैन्य शक्ति को मजबूत किया।
कूटनीतिक चालें और सैन्य विजय
हैदर अली ने न केवल सैन्य बल का निर्माण किया, बल्कि कूटनीतिक चालों में भी माहिर हो गया। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए रणनीतिक रूप से अपने कदम उठाता था। साल 1761 से 1763 तक, हैदर अली ने होस्कोटे, डोड बेलापुर, सेरा, बेदनूर आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और दक्षिण भारत के पोलिगरों (दक्षिण भारत के सामंती सरदार) को अपने अधीन कर लिया।
मराठों से संघर्ष और विजय
मराठों ने पानीपत के तीसरे युद्ध (1761) से जल्दी ही उबर कर पेशवा माधव राव के नेतृत्व में मैसूर पर लगातार आक्रमण किया। साल 1764, 1766 और 1771 में, हैदर अली को इन आक्रमणों में पराजित होना पड़ा। इन हारों के बाद, हैदर अली को मराठों से कुछ क्षेत्रों को सौंपकर उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए धन का भुगतान करना पड़ा।
हालाँकि, 1772 में पेशवा माधव राव की मृत्यु के बाद पुणे में राजनीतिक उलझन का फायदा उठाते हुए हैदर अली ने 1774-76 के बीच सभी क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया, जिन्हें पहले मराठों को सौंपा गया था। साथ ही, उसने बेल्लारी, कडप्पा, गूटी, कर्नूल और कृष्णा-तुंगभद्र डोआब के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी कब्ज़ा कर लिया।
इस प्रकार, हैदर अली के नेतृत्व में, मैसूर ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक शक्ति को मजबूत किया। उनके द्वारा अपनाई गई सैन्य रणनीतियाँ और कूटनीतिक चालें न केवल मैसूर को एक प्रमुख शक्ति बना दिया, बल्कि उन्होंने भारत के दक्षिणी हिस्से में राजनीतिक और सैन्य प्रभाव की दिशा भी बदल दी। हैदर अली के सैन्य कौशल और कूटनीतिक रणनीतियों ने उसे एक महान शासक बना दिया।

प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767-69)
यह कहानी 1767 के समय की है, जब भारतीय उपमहाद्वीप में कई शक्तिशाली राज्य एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। दक्षिण भारत में, मैसूर राज्य के शासक, हैदर अली, अपनी ताकत और क्षेत्रीय महत्व को महसूस करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत परेशान थे। वह जानते थे कि अगर अंग्रेजो ने दक्षिण भारत में अपना कब्जा बढ़ा लिया, तो यह उनके राज्य के लिए खतरे की घंटी हो सकती थी। इसलिए, हैदर अली ने तय किया कि वह इस खतरे का सामना करेंगे और ब्रिटिशों को हराने के लिए एक बड़ा संघर्ष शुरू करेंगे।
अंग्रेजों का भारत में प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने पहले ही बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और अब उनका ध्यान दक्षिण भारत पर था। अंग्रेजों ने अपनी सफलताओं से अंधे होकर 1766 में निज़ाम अली से एक संधि की। इसके तहत अंग्रेजों ने निज़ाम की मदद के लिए सैनिक भेजने का वादा किया। बदले में, निज़ाम ने उत्तरी सरकार का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया।
मद्रास (अब चेन्नई) में ब्रिटिशों का बड़ा आधार था, और उन्होंने कर्नाटका और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में अपने किले बना लिए थे। यह देखते हुए, हैदर अली ने ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया।
इस समय, हैदर अली पहले ही आर्कोट के शासक और मराठों से संघर्ष कर रहे थे। अचानक, निज़ाम, मराठों और कर्नाटिक के नवाब का संयुक्त मोर्चा उनके खिलाफ खड़ा हो गया।
फिर भी, हैदर ने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने मराठों को अपने पक्ष में किया और निज़ाम को कुछ क्षेत्रों का वादा करके उसे अपनी ओर खींच लिया। उस समय मराठा साम्राज्य, जो दक्षिण और मध्य भारत में एक बड़ी शक्ति था, भी युद्ध में शामिल था, लेकिन उनका रुख इस समय पूरी तरह से साफ नहीं था। हालांकि, मराठों का मानना था कि अगर ब्रिटिशों को दक्षिण में फैलने से रोका जाए, तो उनके राज्य को फायदा होगा। मराठों ने न केवल अपने क्षेत्र की रक्षा करने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने हैदर अली से समर्थन भी प्राप्त करने की कोशिश की।
इस बीच, फ्रांसीसी, जो उस समय भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ने हैदर अली से संपर्क किया। फ्रांसीसी लोगों ने ब्रिटिशों के खिलाफ अपनी सेना का समर्थन देने का वादा किया। वे जानते थे कि अगर ब्रिटिशों को दक्षिण भारत में हराया जा सकता है, तो इससे उनकी अपनी ताकत बढ़ सकती है।
युद्ध की शुरुआत 1767 में हुई। अंग्रेजो ने हैदर अली पर हमला किया और कर्नाटका के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया। लेकिन हैदर अली ने अपनी बहादुरी और रणनीति से ब्रिटिशों को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और युद्ध के मैदान में शानदार रणनीतियों का इस्तेमाल किया।
डेढ़ साल तक युद्ध चला, लेकिन अंत में, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया और मद्रास के दरवाजे तक पहुँच गए। घबराए हुए मद्रास सरकार ने अप्रैल 1769 में एक संधि की। मद्रास की संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के क्षेत्रों की बहाली की और एक रक्षात्मक गठबंधन स्थापित किया।
हालांकि युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, लेकिन इसने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार इतना आसान नहीं था। इस युद्ध ने भारतीय शासकों को यह सिखाया कि अगर वे ब्रिटिशों के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे, तो वे उन्हें अपनी जमीन पर कब्जा करने से नहीं रोक पाएंगे।
पहले आंग्ल-मैसूर युद्ध ने यह भी दिखा दिया कि फ्रांसीसी, मराठा, निजाम और ब्रिटिश जैसे विदेशी ताकतों के बीच संघर्ष से भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। यह युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें भविष्य में कई और संघर्षों और संघर्षों का रास्ता साफ हुआ।
(कर्नाटक युद्धों को विस्तार से जानने के लिए क्लिक करें)

दूसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780-84)
दूसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध 1780-84 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर के राज्य के बीच हुआ। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाला महत्वपूर्ण संघर्ष था। इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई।
युद्ध का प्रारंभ: माहे बंदरगाह पर विवाद
ब्रिटिश गवर्नर-जनरल वॉरेन हैस्टिंग्स ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को जब्त करने का आदेश दिया, जिसमें माहे बंदरगाह भी शामिल था। हैदर अली ने इस बंदरगाह को अपनी क्षेत्रीय जिम्मेदारी माना और इसे फ्रांसीसी हमलों से बचाने के प्रयास किए। ब्रिटिशों को डर था कि यह बंदरगाह फ्रांसीसी मदद प्राप्त करने के लिए हैदर अली द्वारा उपयोग किया जा सकता है, जिससे युद्ध और भी बढ़ सकता था।
इसके अलावा, अंग्रेजों ने बिना अनुमति के उनके क्षेत्र से अपनी सेना को गुजरने दिया, जिससे हैदर अली को और भी गुस्सा आया। इस कारण हैदर अली ने मराठों, निजाम और फ्रांसीसी सहायता प्राप्त की और 1780 में कर्नाटिक पर हमला किया।
हैदर अली की विजय और ब्रिटिश हार
हैदर अली ने अर्कोट पर कब्जा कर लिया और सर हेक्टर मुनरो की अगुवाई में भेजी गई ब्रिटिश सेना को हराकर उसे नष्ट कर दिया। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ हैदर अली और मराठों दोनों के खिलाफ युद्ध में थी, और दोनों मोर्चों पर हार का सामना किया।
अल्फ्रेड ल्याल के अनुसार, “1780 की गर्मियों तक, भारत में अंग्रेजों का भाग्य अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच चुका था।”
ब्रिटिश रणनीति और निर्णायक लड़ाइयाँ
हालांकि, ब्रिटिश गवर्नर-जनरल वॉरेन हैस्टिंग्स की सक्रिय नीतियों ने स्थिति को संभाला। कोलकाता से जनरल सर एयर कूट की अगुवाई में एक सेना भेजी गई, जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो (1781) और अरनी (1782) की लड़ाइयों में हराया। साथ ही, मराठों को सिंधिया के साथ समझौते के द्वारा संघर्ष से बाहर कर दिया गया।
फ्रांसीसी सहायता और युद्ध का मोड़
1782 में, फ्रांसीसी एडमिरल बैली डे सुफ्रेन की अगुवाई में फ्रांसीसी सहायता भारत पहुँची, लेकिन ब्रिटिश एडमिरल ह्यूजेस ने उन्हें नष्ट करने की कोशिश की। इसके परिणामस्वरूप, फ्रांसीसी मदद से हैदर अली को बहुत बड़ी सहायता नहीं मिल सकी।
अंग्रेजों के लिए सौभाग्य की बात यह रही कि हैदर अली की दिसंबर 1782 में मृत्यु हो गई। इस घटना ने स्थिति को बदल दिया। उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, हालांकि, 1783 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के खत्म होने की खबर मिली। इसके बाद सुफ्रेन यूरोप वापस लौट गए और टीपू को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया।
मंगलोर की संधि और युद्ध का अंत
मद्रास के अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड जॉर्ज मैकार्टनी ने शांति की ओर रुख किया, और मार्च 1784 में मंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे की ज़मीनों का आदान-प्रदान और युद्ध बंदियों की वापसी का निर्णय लिया गया। इस संघर्ष का परिणाम एक ड्रॉ के रूप में हुआ।
दूसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध 1780-84 भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें ब्रिटिश और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच घमासान संघर्ष हुआ। इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति को कमजोर किया और टीपू सुल्तान की वीरता को भी दुनिया के सामने लाया।

तीसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध (1790-92): एक ऐतिहासिक संघर्ष
ब्रिटिश साम्राज्यवाद, हमेशा शांति संधियों को एक नए हमले का अवसर मानता था। 1790 में, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने निज़ाम और मराठों से मिलकर टीपू के खिलाफ एक त्रिकोणीय गठबंधन किया। इसके कारण, टीपू ने 1784 में तुर्की और फ्रांस से सहायता प्राप्त करने के लिए दूत भेजे थे।
टीपू सुलतान और त्रावणकोर का विवाद
एक और विवाद तब उत्पन्न हुआ जब टीपू ने त्रावणकोर के राजा से युद्ध किया। त्रावणकोर ने डचों से कोचीन राज्य के जैकोटाई और क्रांगनोर क्षेत्रों को खरीदा था, जिसे टीपू ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना। इसके बाद, टीपू ने 1790 में त्रावणकोर पर हमला किया।
ब्रिटिश साम्राज्य का हस्तक्षेप और युद्ध की शुरुआत
अंग्रेज मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार थे। उन्होंने त्रावणकोर के राजा का समर्थन किया और टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। कॉर्नवॉलिस ने बड़ी सेना के साथ बैंगलोर पर हमला किया और मार्च 1791 में इसे जीत लिया। इसके बाद, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर दूसरी बार आक्रमण किया।
1792 की श्रीरंगपट्टनम संधि: टीपू की हार और उसके परिणाम
इस युद्ध में टीपू ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत उसे अपनी ज़मीन का अधिकांश हिस्सा छोड़ना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि (1792) के तहत, अंग्रेजों ने बरामहल, दिंडीगुल और मलाबार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा, मराठों और निज़ाम को भी कुछ क्षेत्रों का लाभ हुआ। इस संधि के अनुसार, टीपू को तीन करोड़ रुपये का युद्ध शुल्क भी चुकाना पड़ा। टीपू ने अपने राज्य के आधे से अधिक क्षेत्र खो दिए, जिससे उसकी शक्ति में कमी आई और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति मजबूत हुई।
तीसरे आंग्ल-मैसूर युद्ध का असर और टीपू की स्थिति
इस युद्ध में टीपू की हार ने ब्रिटिशों को दक्षिण भारत में अपने प्रभाव को और बढ़ाने का मौका दिया। इसके बाद, टीपू ने ब्रिटिशों से मुकाबला जारी रखा, लेकिन उसकी स्थिति कमजोर हो गई थी। इस युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दक्षिण भारत में अपनी सामरिक स्थिति को और सुदृढ़ किया और टीपू सुलतान के साम्राज्य को कमजोर कर दिया।

चौथा आंग्ल-मैसूर युद्ध (1799)
1798 में, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर-जनरल बने। उनका उद्देश्य था या तो टीपू को दबाना या उसकी स्वतंत्रता को समाप्त करना। वेलेस्ली ने ‘सहायक संधि‘ की नीति को अपनाया। इस नीति के तहत, टीपू पर आरोप लगाया गया कि वह निज़ाम, मराठों और फ्रांसीसी के साथ षड्यंत्र कर रहा है।
वेलेस्ली ने इस आरोप का आधार बनाकर टीपू के खिलाफ सैन्य कार्यवाही शुरू की। 17 अप्रैल 1799 को युद्ध शुरू हुआ। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम पर कब्जे के साथ मैसूर की स्वतंत्रता का अंत हो गया। टीपू ने वीरता से लड़ते हुए जान दी।
टीपू के परिवार के सदस्यों को वेल्लोर में बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने कर्नाटिक, कोयंबटूर, वायनाड, धारपुरम और मैसूर के समुद्र तट पर कब्जा कर लिया। कुछ क्षेत्र निज़ाम को दिए गए। अंत में, मैसूर के हिंदू शाही परिवार के एक लड़के कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया गया और सहायक संधि लागू किया गया।
SELECT REFERENCES
1. W.H. Hutton : Marquess Wellesley
2. S.J. Owen : Selection from Wellesley’s Despatches
3. P.Ε. Roberts: India under Wellesley.
4. W.M.Torrens : Marquess Wellesley.
5. Dalrymple William – The Anarchy: The East India Company, Corporate Violence and the Pillage of an Empire
Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.


