रंजीत सिंह के बाद पंजाब
रंजीत सिंह ने अपनी महान नेतृत्व क्षमता से पंजाब में एक सशक्त सिख राज्य की नींव रखी थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वह राज्य स्थिर नहीं रह सका। रंजीत सिंह का शासन सैन्य व्यवस्था पर आधारित था, और उनका तानाशाही तरीका था। जैसा अक्सर किसी व्यक्ति के निधन के बाद होता है, रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी सेना बिखर गई। उनकी बनाई सिख राज्य की भी समाप्ति हो गई। उनकी मौत से खाली जगह नहीं, बल्कि एक शून्य बन गया। इस कारण सिख राज्य की पूरी संरचना डूब गई। इस लेख में हम देखेंगे कि रंजीत सिंह के बाद पंजाब में क्या घटनाएँ घटीं, किस तरह से सत्ता संघर्ष हुआ और आखिरकार कैसे एंग्लो-सिख युद्धों ने सिख साम्राज्य के पतन में योगदान दिया।
रंजीत सिंह के बाद राज्य में अराजकता का दौर
रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद, पंजाब में अराजकता और भ्रम का माहौल बन गया। धीरे-धीरे सारी असली शक्ति खालसा सेना के हाथों में चली गई। रंजीत सिंह ने 40,000 सैनिकों की एक बड़ी स्थायी सेना छोड़ी थी, जो राज्य के घटते संसाधनों पर भारी दबाव बन गई।

रंजीत सिंह की मृत्यु के पांच साल बाद, उनकी सेना की ताकत तीन गुना बढ़ गई, और यह राज्य के घटते संसाधनों पर भारी दबाव बन गई। जब सैनिकों को उनकी तनख्वाह नहीं दी जा सकी, तो वे बेख़ौफ़ हो गए। वे राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और तनख्वाह बढ़ाने के लिए शाही दावेदारों से सौदेबाजी करने लगे। सैनिकों ने अपनी पंचायतें बनाईं और खुद तय किया कि वे किसी अभियान पर जाएं या नहीं, चाहे सरकार कुछ भी कहे। सेना ने ‘राजा बनाने’ का काम शुरू कर दिया और सरकार की शक्ति कम कर दी।
इसके अलावा, रंजीत सिंह ने जिन शक्तिशाली जागीरदारों को कड़ा नियंत्रण में रखा था, वे अब बेकाबू हो गए। पंजाब एक संघर्ष और सत्ता की लड़ाई का मैदान बन गया। रंजीत सिंह के कमजोर और अयोग्य बेटे, जिनकी वैधता भी सवालों के घेरे में थी, अराजकता को संभाल नहीं पाए। एक आलोचक ने इसे इस तरह कहा: “साजिशें जागीरदारों के दिमाग में थीं, सेना शक्ति थी और सिंहासन के दावेदार केवल मोहरे थे।” रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद, पंजाब का इतिहास साजिशों, हत्याओं, विश्वासघातों और अराजकता से भरा हुआ बन गया, जिससे राज्य की स्थिरता पूरी तरह से टूट गई।
खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह का शासन संघर्ष
रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद, उनका पुत्र खड़क सिंह महाराजा बना। लेकिन खड़क सिंह एक नशेड़ी और अयोग्य शासक थे। जल्द ही, संधवालिया और डोगरा सरदारों के गुटों ने राज्य में अराजकता फैला दी। 8 अक्टूबर 1839 को, रंजीत सिंह के प्रिय चेहत सिंह को वजीर ध्यान सिंह के किराए के हत्यारों ने मार डाला। इसके बाद खड़क सिंह को जेल में डाल दिया गया और नौनिहाल सिंह को महाराजा घोषित किया गया।
नौनिहाल सिंह ने सत्ता संभालते हुए कुछ सुधार किए। उन्होंने राज्य में कानून और व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की। उन्होंने मंडी और सुकेत के पहाड़ी राज्यों को नियंत्रित किया और लद्दाख तथा बलतिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। लेकिन दुर्भाग्यवश, नौनिहाल सिंह की मृत्यु 5 नवम्बर 1840 को हुई। वह एक दुर्घटना में घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
सत्ता संघर्ष और शेर सिंह का उभार
नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद, डोगरा और संधवालिया सरदारों ने फिर से सत्ता के लिए संघर्ष किया। संधवालिया सरदारों ने नौनिहाल सिंह की मां माई चंद कौर के पक्ष में समर्थन जुटाया, जो अपने मृत बेटे के स्थान पर संरक्षक बनना चाहती थीं। वहीं, डोगरा सरदारों ने रंजीत सिंह के दूसरे पुत्र शेर सिंह को समर्थन दिया। शेर सिंह ने सिख सेना की मदद से सफलता हासिल की और जनवरी 1841 में महाराजा घोषित हुए। डोगरा ध्यान सिंह को वजीर बनाया गया और संधवालिया सरदार ब्रिटिशों के पास शरण लेने चले गए।
शेर सिंह ने संधवालिया सरदारों को शांत करने के लिए उन्हें अपनी कृपाएं दीं। लेकिन सितंबर 1843 में अजीत सिंह संधवालिया ने धोखाधड़ी से शेर सिंह को गोली मार दी और वजीर ध्यान सिंह को भी मार डाला। ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह ने बदला लिया और वेतन बढ़ाने का वादा करते हुए सेना का समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने संधवालिया सरदारों, लेहना सिंह और अजीत सिंह की हत्या कर दी।

दलीप सिंह और वजीरों की स्थिति
सितंबर 1843 में, रंजीत सिंह के छोटे पुत्र दलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया। रानी जिंदन को संरक्षक बनाया गया और हीरा सिंह डोगरा को वजीर नियुक्त किया गया। लेकिन हीरा सिंह भी सत्ता संघर्ष का शिकार बने और 21 दिसम्बर 1844 को उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद, जवाहार सिंह, जो रानी जिंदन के भाई थे, वजीर बने। लेकिन उनका भी भाग्य अच्छा नहीं था। सेना के गुस्से का शिकार होकर उन्हें 1845 में पदच्युत कर दिया गया और मार दिया गया।
इसके बाद, लाल सिंह, जो रानी जिंदन के प्रेमी थे, ने सेना का समर्थन प्राप्त किया और वजीर बने। तेजा सिंह को सेना का नया कमांडर नियुक्त किया गया।
पंजाब की अस्थिरता और अंग्रेजों का आक्रमण
पंजाब में सत्ता संघर्ष और अस्थिरता का माहौल बढ़ता गया। इस दौरान, अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण करने की योजना बनाई। रानी जिंदन और उनके समर्थक लाल सिंह के नेतृत्व में पंजाब ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि, स्थिति ने इतनी तेजी से बदलती कि अंततः 1845 में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया और सिख राज्य का अंत कर दिया।
इस प्रकार, रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में स्थिति पूरी तरह से अस्थिर हो गई। सिख राज्य के अंदर साजिशों, हत्याओं, और सत्ता संघर्षों का दौर चला, जिसके कारण अंग्रेजों ने आसानी से पंजाब पर कब्जा कर लिया और सिख साम्राज्य का अंत हुआ।

पहला एंग्लो-सिख युद्ध, 1845-46
ब्रिटिशों की नजरें हमेशा पंजाब में हो रही घटनाओं पर बनी हुई थीं। वे सतलज नदी के पार उपजाऊ मैदानों पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। मई 1838 में W.G. Osborne ने लिखा था, “रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद, पंजाब पर कब्जा करने का रास्ता खुल सकता है और हमारी सीमा सिंधु नदी तक बढ़ सकती है।” इस समय ब्रिटिश राजनेता और सैन्य अधिकारी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि पंजाब पर कब कब्जा किया जाए। हालांकि, अफगानिस्तान में ब्रिटिशों के उलझने के कारण, उनकी योजनाओं में देरी हुई। 1841 में, सर विलियम मैकनेटन ने लॉर्ड ऑकलैंड को लिखा, “हमें पंजाब पर कब्जा करना चाहिए, ताकि हम पेशावर तक पहुंच सकें।” अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना की असफलता ने ब्रिटिश प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया था। इसके बाद, ब्रिटेन ने सिंध और पंजाब के शासकों के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की।
1843 में, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो ने ब्रिटिश साम्राज्य को और मजबूत करने के लिए पंजाब का अधिग्रहण जरूरी बताया। उन्होंने कहा, “पंजाब हमारे नियंत्रण में होगा, यह तो निश्चित है, बस समय का इंतजार करना है।”
ब्रिटिश तैयारियां
लॉर्ड एलेनबरो के बाद, 1844 में लॉर्ड हेनरी हार्डिंग गवर्नर जनरल बने। उन्होंने ब्रिटिश सेना की स्थिति मजबूत करने के लिए कदम उठाए। कंपनी की सेना को बढ़ाकर 32,000 सैनिकों तक किया गया, जिसमें 68 तोपें भी शामिल थीं। इसके अलावा, कंपनी ने सतलज नदी पर पुल बनाने के लिए 57 नावें भेजी। सेना को यह भी ट्रेनिंग दी गई कि वे पुल बनाने में सक्षम हों। दूसरी ओर, सिखों ने इन तैयारियों को देखा और समझ लिया कि यह सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, बल्कि आक्रमण के लिए किया जा रहा था।
ब्रॉडफुट का हस्तक्षेप
1843 में, मेजर ब्रॉडफुट को लुधियाना में ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया। वह सिखों के मामलों में हस्तक्षेप करते थे, जिससे एंग्लो-सिख संबंध और बिगड़े। उन्होंने लाहौर दरबार को चुनौती दी और घोषणा की कि सतलज के पार की सारी ज़मीनें ब्रिटिश नियंत्रण में हैं। इसके अलावा, आनंदपुर के साधु-पुजारियों के मामलों में भी उनका हस्तक्षेप हुआ। इसके कारण सिखों के बीच असंतोष बढ़ा।
युद्ध की शुरुआत
ब्रिटिशों की गतिविधियों से सिखों को यह एहसास हुआ कि यह युद्ध का समय आ चुका है। 11 दिसंबर 1845 को, सिख सैनिकों ने सतलज नदी पार की और अंग्रेजों पर हमला किया। 13 दिसंबर 1845 को, हेनरी हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा की और यह भी बताया कि महाराजा दलीप सिंह का कब्जा, जो सतलज के बाएं किनारे पर था, अब ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया गया। लाल सिंह, जो सिख सेना के कमांडर-इन-चीफ थे, ने विश्वासघात किया और अंग्रेजों को यह संदेश भेजा कि वह अपनी सेना को दो दिन के लिए वापस बुलाने का आदेश देंगे।
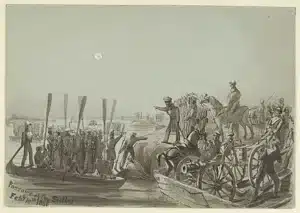
युद्ध और परिणाम
सिख और ब्रिटिश सैनिकों के बीच कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, जिनमें मुड़की, फिरोजेशाह, बुड्डेवाल और अलीवाल शामिल थे, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। आखिरकार, 10 फरवरी 1846 को सोबरोन की लड़ाई निर्णायक साबित हुई। इस युद्ध में सिख सैनिकों की भारी हताहत हुई, क्योंकि लाल सिंह और तेजा सिंह ने अंग्रेजों को खाइयों की सभी जानकारी दे दी थी।
ब्रिटिशों ने सतलज नदी पार की और लाहौर पर कब्जा कर लिया। 9 मार्च 1846 को, रंजीत सिंह की राजधानी में शांति शर्तें लागू कर दी गईं। समझौते के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे:
1. महाराजा ने सतलज नदी के दक्षिण स्थित क्षेत्रों से सभी संबंधों और दावों को त्याग दिया।
2. सिखों के किलों, क्षेत्रों और अधिकारों को ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपा गया।
3. युद्ध के मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपये की मांग की गई, जिसे सिख दरबार ने असमर्थता के बावजूद स्वीकार किया।
4. सिख सेना को 20,000 पैदल सैनिकों और 12,000 घुड़सवारों तक सीमित किया गया।
5. लाहौर में ब्रिटिश सैनिकों को स्वतंत्र रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
6. नाबालिक दलीप सिंह को महाराजा के रूप में मान्यता दी गई और रानी जिंदन को रीजेंट नियुक्त किया गया।
7. सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश निवासी के रूप में नियुक्त किया गया।
समझौते के बाद की स्थिति
11 मार्च 1846 को हुए एक समझौते के तहत, वज़ीर लाला सिंह और अन्य के कहने पर, एक ब्रिटिश सेना को लाहौर में 1846 के अंत तक रखा जाएगा। इसका उद्देश्य महाराजा और लाहौर के लोगों की सुरक्षा करना और सिख सेना का पुनर्गठन करना था। लाहौर किला अब ब्रिटिश सेना के लिए खाली कर दिया गया, और लाहौर दरबार को कंपनी की सेना के खर्चों को उठाना होगा।
ब्रिटिशों की योजना और भविष्य
फरवरी 1846 में पंजाब को ब्रिटेन में शामिल नहीं किया गया था, और यह विचार कि इसे रंजीत सिंह की याद में जोड़ा नहीं गया, शायद सही नहीं था। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों का मानना था कि लॉर्ड हेनरी हार्डिंग ने “सावधानी से “ काम किया था। लेकिन अगर हम घटनाओं को गहराई से देखें, तो यह पता चलता है कि पंजाब का अधिग्रहण ब्रिटिशों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर रहा था। हालांकि, खालसा सेना को हराया गया था, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया था। लाहौर और अमृतसर में 25,000 सिख सैनिक थे और पेशावर में 8,000। इसके अलावा, हर सिख किसान के पास हथियार थे, जिससे गुरिल्ला युद्ध की संभावना बनी रहती थी। इसके अलावा, भारतीय खजाने में कमी थी और गर्मी का मौसम भी पास आ रहा था। इस स्थिति में, एक समझदारी से और संयम वाली नीति सबसे सही लग रही थी। फिर भी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पंजाब को कमजोर करने के लिए कड़े कदम उठाए, जिससे उसका पूरा अधिग्रहण समय की बात बन गई। पंजाब राज्य को छोटा किया गया, सैन्य रूप से कमजोर किया गया और वित्तीय तौर पर दबाया गया। असल में, ब्रिटिशों का असली मकसद इस पत्र से साफ हो जाता है, जो लॉर्ड हेनरी हार्डिंग ने 23 अक्टूबर 1847 को हेनरी लॉरेंस को लिखा था: “हमारे द्वारा उठाए गए सभी कदमों में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मार्च 1846 के लाहौर समझौते के अनुसार पंजाब कभी भी स्वतंत्र राज्य नहीं था… असल में, स्थानीय शासक अब हमारे नियंत्रण में हैं और उन्हें हमारी इच्छाओं के अनुसार काम करना होगा।”
पहला एंग्लो-सिख युद्ध 1845-46 ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य की दृष्टि में पंजाब का अधिग्रहण अपरिहार्य था। हालांकि, युद्ध में दोनों पक्षों ने काफी संघर्ष किया, लेकिन अंत में ब्रिटिशों ने अपनी शक्ति को साबित किया और लाहौर पर कब्जा किया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप सिख साम्राज्य की स्थिति और कमजोर हो गई, और पंजाब धीरे-धीरे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया।
दूसरा एंग्लो-सिख युद्ध, 1848-49: एक ऐतिहासिक विश्लेषण
दूसरा एंग्लो-सिख युद्ध, जो 1848-49 में हुआ, वह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध था। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और सिखों के बीच लड़ा गया और इसके परिणामस्वरूप सिखों का स्वतंत्रता संग्राम विफल हो गया। इस लेख में हम इस युद्ध के कारणों, घटनाओं और परिणामों का विश्लेषण करेंगे।
ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार और सिखों का विरोध
लाहौर संधि (1846) के बाद कुछ महीनों में रानी जिंदन और लाल सिंह को यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों के वास्तविक इरादे उनके खिलाफ थे। जब रेजिडेंट ने लाहौर दरबार से कश्मीर के राजा गुलाब सिंह को सौंपने का आदेश दिया, तो लाल सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से इमाम-उद-दीन (कश्मीर के मुस्लिम गवर्नर) को इस आदेश का विरोध करने के लिए उकसाया। इसके परिणामस्वरूप, अंग्रेज़ों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया।
लाल सिंह को इस मामले में साजिश का दोषी ठहराया गया और उन्हें कोर्ट ऑफ इनक्वायरी द्वारा दोषी पाया गया। उन्हें निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद, लाहौर दरबार का प्रशासन एक रीजेंसी काउंसिल को सौंपा गया, जिसमें फकीर नूर-उद-दीन, तेजा सिंह, शेर सिंह और दीना नाथ जैसे प्रमुख सदस्य थे।
लाहौर संधि और ब्रिटिश दबाव
1846 के बाद, ब्रिटिश रेजिडेंट ने लाहौर दरबार से यह वादा लिया कि वह कुछ वर्षों तक लाहौर में ब्रिटिश सैनिकों को तैनात रखेंगे। इसके लिए 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल में एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि में लाहौर दरबार ने ब्रिटिश सैनिकों के खर्चों को उठाने के लिए प्रति वर्ष 22 लाख रुपये देने की सहमति दी।
महाराजा दलीप सिंह की नाबालिग अवस्था के दौरान, वास्तविक प्रशासन ब्रिटिश रेजिडेंट और आठ प्रमुखों की काउंसिल द्वारा किया जाता था, जिससे ब्रिटिश रेजिडेंट पंजाब का वास्तविक शासक बन गया। जब महारानी जिंदन ने इस स्थिति का विरोध किया, तो उन्हें शेखुपुरा भेज दिया गया और उनका भत्ता 48,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया।
डलहौजी का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण
1848 में डलहौजी ने गवर्नर-जनरल के रूप में पदभार संभाला। डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य के एक प्रमुख विस्तारवादी थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार को हर उचित अवसर का उपयोग करना चाहिए और पंजाब के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए।
मुलराज का विद्रोह और सिखों का संघर्ष
मुलराज, जो मुल्तान के गवर्नर थे, ने ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों द्वारा कठोर शर्तों को लागू करने के खिलाफ विद्रोह किया। 1847 में उन्हें 20 लाख रुपये का नजराना देने और राजस्व में एक तिहाई वृद्धि करने का आदेश दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने इन शर्तों को मानने से इंकार किया, तो उनका इस्तीफा ले लिया गया। मार्च 1848 में, ब्रिटिश रेजिडेंट फ्रेडरिक करी ने काहन सिंह मन को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया। लेकिन वहाँ के सिख सैनिकों और नागरिकों ने विद्रोह कर दिया।
यह विद्रोह बहुत जल्दी एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया, जिसमें चतर सिंह और शेर सिंह जैसे सिख नेता शामिल हुए। सिखों ने अफगानों से दोस्ती करने के लिए पेशावर का अंशदान भी किया। अब यह संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बड़े संघर्ष में बदल गया।

युद्ध की घटनाएँ और अंग्रेजों की जीत
मुल्तान में हुई लड़ाई के बाद, सिखों ने चिलियानवाला और गुजराट में भी अंग्रेजों से मुकाबला किया। हालांकि, अंग्रेजों ने अंततः सिखों को पराजित किया। 16 नवंबर 1848 को रावी पार किए जाने के बाद, 1849 में सिखों को गुजराट में निर्णायक हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद, ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया।
डलहौजी का पंजाब का अधिग्रहण (H3)
डलहौजी के पास तीन विकल्प थे:
1. पंजाब की स्थिति को यथावत रखना।
2. केवल मुल्तान का अधिग्रहण करना और मुलराज को सजा देना।
3. पूरे पंजाब का अधिग्रहण करना।
डलहौजी ने तीसरे विकल्प को चुना और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संरक्षित करना “मजाक” होगा। 29 मार्च 1849 को गवर्नर-जनरल की घोषणा में कहा गया, “पंजाब का राज्य समाप्त हो गया है और महराजा दलीप सिंह की सभी भूमि अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है।”
दूसरा एंग्लो-सिख युद्ध 1848-49 ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। इस युद्ध ने सिखों के संघर्ष और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। इसके परिणामस्वरूप, पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया, और सिखों के शासक, महाराजा दलीप सिंह, को अपनी भूमि से वंचित कर दिया गया।
निष्कर्ष
रंजीत सिंह के बाद पंजाब में अराजकता का दौर शुरू हुआ, और यह सिख साम्राज्य धीरे-धीरे कमजोर होने लगा। सत्तारूढ़ संघर्ष, धोखाधड़ी, और शाही परिवार के भीतर चल रही साजिशों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इसके कारण अंग्रेजों के लिए पंजाब पर कब्जा करना आसान हो गया। पहले एंग्लो-सिख युद्ध के बाद सिखों को हार मिली, और दूसरे युद्ध में तो सिख साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस तरह, रंजीत सिंह के शासन के बाद पंजाब की स्थिति में आई गिरावट ने सिख साम्राज्य के अंत का मार्ग प्रशस्त किया, और पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम ने भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को नया दिशा दी।
SELECT REFERENCES
1. А. С. Banerjee : Anglo-Sikh Relations
2. Jagmohan Mahajan : History of the Panjab
3. J. D. Cunningham : History of the Sikhs
4. M. Latif : History of the Panjab
5. Evans Bell : Annexation of the Punjab
Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.


